Bharati Bhawan Class 10 Biology Chapter 7 Questions Answer | दीर्घ उत्तरीय प्रश्र | अनुवांशिकता तथा जैव विकास | Heredity and Evolution
भारती भवन जीवविज्ञान कक्षा 10 अध्याय - 7 ; अनुवांशिकता तथा जैव विकास
1. विभिन्नता क्या है? जननिक विभिन्नता एवं कायिक विभिन्नता का वर्णन करें।
उत्तर : विभिन्नताएँ :—
➥ एक ही प्रकार के जनकों उत्पन्न विभिन्न संतानों में कुछ न कुछ अंतर निश्चित रूप में रहता है , जैसे — रंग– रूप, शरीर का गठन , आवाज, आदि । एक ही प्रजाति के जीवों में दिखनेवाले ऐसे अंतर आनुवांशिक अंतर या वातावरणीय दशाओं में अंतर के कारण होते है । एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जानेवाले इन्हीं अंतरों को विभिन्नता कहते है
विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो उसे अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता को दर्शाते हैं।
विभिन्नताओं के प्रकार :—
विभिन्नताएँ दो प्रकार की होती है
(i) जननिक
(ii) कायिक
(i) जननिक विभिन्नताएँ :—
➥ ऐसी विभिन्नताएँ जनन-कोशिकाओं में होनेवाले परिवर्तन के कारण होती हैं। ऐसी विभिन्नताएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती हैं। इस कारण से जननिक विभिन्नता आनुवंशिक विभिन्नता भी कहलाती है , आनुवांशिक विभिन्नता क्रोमोसोम के पर जीन की व्यवस्था में परिवर्तन तथा DNA के निर्माण संलग्न नाइट्रोजेनी क्षार के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है
जैसे : आंखों का रंग ,बालों का रंग शरीर की लंबाई आदि
(ii) कायिक विभिन्नताएँ :-
➥ ऐसी विभिन्नताएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होती हैं। इनका जैव विकास में महत्त्व नहीं होता है।
2. मेंडल द्वारा मटर पर किए गए एकसंकर संकरण के प्रयोग तथा निष्कर्ष का वर्णन करें।
उत्तर : ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर एकसंकर संकरण का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने एक गुण के दो विपरीत लक्षणों — जैसे लंबा (Tall) और बौना (Dwarf) — का अध्ययन किया। उन्होंने शुद्ध लंबे पौधों (TT) के परागकणों से शुद्ध बौने पौधों (tt) का परागण किया। इस क्रॉस को जनक पीढ़ी (P) कहा गया। इस प्रकार के परागण (pollination) के बाद जो बीज बने उनसे उत्पन्न सारे पौधे लंबे नस्ल के हुए। इस पीढ़ी के पौधों को मेंडल ने प्रथम संतति (first filial generation) कहा तथा इन्हें F1 अक्षर से इंगित किया
F₁ पीढ़ी (प्रथम संतति):
➥ F₁ पीढ़ी के सभी पौधे लंबे (Tt) हुए, क्योंकि लंबा लक्षण प्रभावी था और बौना लक्षण अप्रभावी | इसलिए सभी पौधे लंबे दिखे लेकिन वे संकर नस्ल के थे (Tt)।
F₂ पीढ़ी (द्वितीय संतति):
➥ जब F₁ पीढ़ी के पौधों को आपस में प्रजनित किया गया, तो F₂ पीढ़ी में पौधों का अनुपात निम्नलिखित मिला:
लक्षणप्ररूपी अनुपात — 3 : 1
जीनप्ररूपी अनुपात — 1 : 2 : 1
निष्कर्ष :
(i) गुण अपने आप में नष्ट नहीं होते, बल्कि अगली पीढ़ियों में पुनः प्रकट हो सकते हैं।
(ii) प्रभावी गुण अप्रभावी गुण पर हावी रहता है।
(iii) यह प्रयोग मेंडल के पृथक्करण के नियम को सिद्ध करता है।
(iv) इस प्रयोग को एकसंकर संकरण कहा गया क्योंकि इसमें केवल एक जोड़े विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया गया था।
3. मनुष्य में लिंग-निर्धारण के विधि का वर्णन करें।
उत्तर : मनुष्य में लिंग-निर्धारण क्रोमोसोम द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े (कुल 46) क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े ऑटोसोम (autosomes) कहलाते हैं और 23वां जोड़ा लिंग-क्रोमोसोम (sex chromosomes) होता है।
लिंग-क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं—X और Y। मादा में दो X क्रोमोसोम (XX) होते हैं, जबकि नर में एक X और एक Y क्रोमोसोम (XY) होता है। युग्मकों (gametes) के निर्माण के समय, मादा केवल X क्रोमोसोम वाले अंडाणु बनाती है, जबकि नर दो प्रकार के शुक्राणु बनाता है—एक में X और दूसरे में Y क्रोमोसोम होता है।
जब शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है , यदि अंडाणु में X क्रोमोसोम और शुक्राणु में X क्रोमोसोम मिले, तो शिशु मादा (XX) बनेगा। और यदि अंडाणु में X और शुक्राणु में Y क्रोमोसोम मिले, तो शिशु नर (XY) बनेगा। इस प्रकार, लिंग-निर्धारण की ज़िम्मेदारी नर के शुक्राणु पर होती है, और इस प्रक्रिया को हेटेरोगैमेसिस (Heterogamety) कहा जाता है।
4. जैव विकास क्या है? लामार्कवाद का वर्णन करें।
उत्तर : जैव विकास :–
➥ जैव विकास जीवविज्ञान की वह शाखा है जिसमे जीवों की उत्पति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा उसमे समय–समय पर क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है
पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकाश प्रारंभ में पाए जानेवाले सरल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार परिवर्तनों के कारण हुआ। सजीव जगत में होनेवाली इस परिवर्तन को जैव विकास कहते है
लैमार्कवाद :
➥ लैमार्क का सिद्धांत 1809 ई० में उनकी पुस्तक "फिलॉसफी जुडोजीक" (Philosophic Zoologique) में प्रकाशित हुआ।
इस सिद्धांत के अनुसार :
➥ जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे "अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत" भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशगति होती है, जिसके फलस्वरूप नयी-नयी जातियाँ बन जाती हैं। उदाहरण-जिराफ की गर्दन का लंम्बा होना
5. डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का वर्णन करें।
उत्तर : डार्विनवाद :
➥ डार्विन ने जैव विकास की व्याख्या अपनी पुस्तक the origin of Species मे व्यक्त किया ।
चार्ल्स डार्विन (1809-1882 ई०) 1831 ई० में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया।
डार्विनवाद के अनुसार :
➥ सभी जीवों में प्रचुर सन्तानोत्पत्ति की क्षमता होती है। अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवनपर्यन्त संघर्ष करना पड़ता हैं। ये संघर्ष सजातीय, अन्तर्जातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिलकुल समान नहीं होते। ये विभिन्नताएँ इन्हें इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएँ जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती हैं, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती हैं। जीवों में विभिन्नताएँ वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएँ पीढ़ी-दर-पीढी इकट्ठी होती रहती हैं और काफी समय बाद उत्पन्न जीव धारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है।
6. आनुवंशिक विभिन्नता के स्रोतों का वर्णन करें।
उत्तर : आनुवंशिक विभिन्नता के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं:
(i). आनुवंशिक उत्परिवर्तन :
➥ यह DNA की प्रतिलिपि के निर्माण के समय नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम (sequence) में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। इससे जीन की संरचना में बदलाव आ जाता है, जो संतानों में भिन्नता उत्पन्न करता है।
(ii). आनुवंशिक पुनर्योग :
➥ लैंगिक जनन के समय जब माता-पिता के गुणसूत्रों का संयोग होता है, तब विभिन्न प्रकार के जीनों का पुनः संयोजन होता है, जिससे संतान में नए प्रकार के आनुवंशिक संयोजन बनते हैं।
(iii). क्रोमोसोम पर जीन की व्यवस्था में परिवर्तन:
➥ क्रोमोसोम पर जीन की स्थिति या अनुक्रम में होने वाले बदलाव भी विभिन्नता का कारण बनते हैं।
(iv) . लैंगिक जनन:
➥ लैंगिक जनन में संतान को माता-पिता दोनों से जीन मिलते हैं, जिससे हर संतान में कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है, भले ही वे एक ही माता-पिता से उत्पन्न हों।
7. पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालें।
उत्तर : पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति एक जटिल और वैज्ञानिक विषय है, जिस पर अनेक वैज्ञानिकों ने अपने-अपने मत और प्रयोग प्रस्तुत किए हैं। डार्विन ने जीवों की नई प्रजातियों की उत्पत्ति को पीढ़ी-दर-पीढ़ी होनेवाली विभिन्नताओं के संचयन से जोड़ा, जबकि मेंडल ने गुणों के वंशागत होने की व्याख्या की। लेकिन यह प्रश्न कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, वैज्ञानिकों के लिए एक गूढ़ विषय रहा है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि जब पृथ्वी पर जीवन के चिह्न नहीं थे, तभी कुछ रासायनिक क्रियाएँ पृथ्वी के आदिम वातावरण में प्रारंभ हुईं। प्रारंभ में लघु अणुओं जैसे ऐसीटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल आदि से एमीनो अम्ल, लिपिड, शर्करा तथा RNA जैसे वृहद अणुओं का निर्माण हुआ। इन्हीं वृहद अणुओं की क्रियाओं से जीवन के लिए आवश्यक जैविक अणुओं की उत्पत्ति संभव हुई।
ओपैरिन, हैल्डेन, मिलर, यूरे तथा सिडने फॉक्स जैसे वैज्ञानिकों ने यह परिकल्पना प्रस्तुत की कि जीवन की उत्पत्ति समुद्र में हुई क्रमिक रासायनिक क्रियाओं के द्वारा लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले हुई। उस समय पृथ्वी का वातावरण अपचायक था, जिसमें मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन जैसी गैसें मौजूद थीं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था।
मिलर और यूरे ने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि उस समय के वातावरण में सरल कार्बनिक अणु जैसे एमीनो अम्ल का निर्माण संभव था। परंतु जब यही प्रयोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया गया तो एमीनो अम्ल नहीं बन पाए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए अपचायक वातावरण आवश्यक था।
इस प्रकार, यह माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर रासायनिक क्रियाओं द्वारा हुई और बाद में विकास की प्रक्रिया से विभिन्न प्रकार के जीवों का निर्माण हुआ।
8. जीवों में जाति-उद्भवन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है?
उत्तर : जीवों में जाति-उद्भवन की प्रक्रिया सूक्ष्मविकास के माध्यम से होती है। एक ही प्रजाति के जीवों में वंशागत विभिन्नताएँ होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती हैं। ये विभिन्नताएँ नई उपप्रजाति के विकास में सहायक होती हैं।
जब किसी प्रजाति की आबादी किसी भौगोलिक अवरोध (जैसे–पहाड़, नदी) के कारण दो उपआबादियों में बँट जाती है, तो उनके बीच जीन प्रवाह रुक जाता है। ऐसी स्थिति में उत्परिवर्तित जीन एक उपआबादी में प्रभावी हो जाते हैं और लाभदायक गुणों के रूप में संतानों में दिखाई देते हैं। प्रकृति ऐसे लाभदायक गुणों का चयन करती है और धीरे-धीरे एक नई उपप्रजाति विकसित हो जाती है।
यदि समय के साथ यह उपप्रजाति मूल प्रजाति से इतनी भिन्न हो जाए कि उनके बीच प्रजनन से संतान उत्पन्न न हो सके या संतान बांझ हो, तो यह प्रक्रिया जाति-उद्भवन कहलाती है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से अंतःप्रजनन, आनुवंशिक विचलन और प्राकृतिक चयन के माध्यम से लैंगिक जनन करनेवाले जीवों में होती है। अलैंगिक जनन या स्व-परागण वाले पौधों में यह प्रक्रिया नहीं हो पाती है ।
Important links
• Bharati bhawan Class 10 Biology All Chapter Solution In Hindi





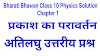




0 Comments