Class 10 Chemistry Chapter 3 – Bharati Bhawan Solution | Long type Short Q&A | दीर्घ उत्तरीय प्रश्र | धातु एवं अधातु |
भारती भवन रसायनशास्त्र कक्षा 10 अध्याय - 3
1. इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्त्वों को धातु एवं अधातु में किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? सोदाहरण समझाएँ।
उत्तर : इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर धातु एवं अधातु का वर्गीकरण
(i) धातु :
➥ धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तत्व अक्रिय गैस जैसी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए अपने संयोजक इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देते हैं। परिणामस्वरूप ये धनायन बनाते हैं।
उदाहरण:
सोडियम (Na):
परमाणु संख्या 11
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास = 2, 8, 1
अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसे खोकर Na⁺ आयन बनाता है।
(ii) अधातु :
➥ अधातुओं के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में सामान्यतः 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अक्रिय गैस जैसी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। परिणामस्वरूप ये ऋणायन बनाते हैं।
उदाहरण:
क्लोरीन (Cl): परमाणु संख्या 17
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास = 2, 8, 7
अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर Cl⁻ आयन बनाता है।
2. कारण सहित बताएँ कि धातुएँ विद्युत की सुचालक और अधातुएँ विद्युत की कुचालक क्यों होती हैं?
उत्तर : धातुओं की बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे रहते हैं और आसानी से निकलकर मुक्त इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। विद्युत विभव लगाने पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा के रूप में प्रवाहित होते हैं। इसलिए धातुएँ अच्छी सुचालक होती हैं।
अधातुओं की बाहरी कक्षा में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मज़बूती से बँधे रहते हैं और आसानी से मुक्त नहीं होते है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है , इसलिए अधातुएँ विद्युत की कुचालक होती हैं।
3. धातुओं के किन्हीं तीन गुणों का उल्लेख करें।
उत्तर : धातुओं के तीन गुण निम्लिखित है –
(i). धातुएँ विद्युत एवं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं।
(ii). धातुएँ आघातवर्धनीय एवं तन्य होती हैं।
(iii). . धातुओं की सतह पर चमक होती है।
4. अधातुओं के किन्हीं तीन गुणों का उल्लेख करें।
उत्तर : अधातुओं के तीन गुण निम्लिखित हैं –
(i). अधातुएँ विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं।
(ii). अधातुएँ भंगुर होती हैं, हथौड़े से मारने पर टूट जाती हैं।
(iii). अधातुओं में चमक नहीं होती, वे प्रायः फीकी दिखाई देती हैं।
5. जस्ता कॉपर सल्फेट के विलयन से ताँबा को विस्थापित कर देता है, किंतु ताँबा जिंक सल्फेट के विलयन से जस्ता को विस्थापित नहीं कर सकता है, क्यों?
उत्तर : जस्ता (Zn) ताँबे (Cu) की तुलना में अधिक क्रियाशील धातु है और यह धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में ताँबे से ऊपर स्थित है। इस कारण जस्ता, कॉपर सल्फेट (CuSO₄) के विलयन से ताँबा को विस्थापित कर देता है :
$Zn + CuSO₄ \rightarrow ZnSO₄ + Cu$
परंतु ताँबा (Cu) जस्ता (Zn) से कम क्रियाशील धातु है और क्रियाशीलता श्रेणी में नीचे स्थित है।
इसी कारण ताँबा, जिंक सल्फेट (ZnSO₄) के विलयन से जस्ता को विस्थापित नहीं कर सकता।
6. द्विधर्मी ऑक्साइड क्या हैं? द्विधर्मी ऑक्साइडों के दो उदाहरण दें।
उत्तर : द्विधर्मी ऑक्साइड :-
➥ कुछ धातुओं के ऑक्साइड (Al2O3, ZnO, PbO, आदि) में अम्लीय एवं भास्मिक दोनों प्रकार के गुण रहते हैं। ये द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये अम्ल एवं भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं।
7. भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें।
उत्तर : भौतिक गुण के आधार पर :–
| धातु | अधातु |
|---|---|
| (i). धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। (ii). धातुएँ प्रायः विद्युत- धनात्मक होती हैं। (iii). धातुएँ प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। (iv). साधारण ताप पर धातुएँ प्रायः ठोस होती हैं। सिर्फ मरकरी (पारा) ही एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव होती है। (v). धातुएँ आघातवर्धनीय तथा तन्य होती हैं। (vi). धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। (vii). हथौड़े से पीटने पर धातुओं से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। |
(i). अधातुओं में ऐसी कोई चमक नहीं होती है। अपवाद - आयोडीन एवं प्रेफाइट में धातुई चमक होती है। (ii). अधातुएँ प्रायः विद्युत- ऋणात्मक होती हैं। सिर्फ हाइड्रोजन विद्युतधनात्मक होता है। (iii). अधातुएँ प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। सिर्फ हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट (अधातुएँ) विद्युत के सुचालक होते हैं (iv). अधातुएँ साधारण ताप पर ठोस या गैस होती हैं। सिर्फ ब्रोमीन (अधातु) साधारण ताप पर द्रव होती है। (v). अधातुएँ आघातवर्धनीय तथा तन्य नहीं होती हैं। अपवाद- प्लास्टिक गंधक तन्य होता है। (vi). अधातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। (vii) . अधातुओं में धातुई ध्वनि नहीं निकलती, बल्कि हथौड़े से पीटने पर अधातुएँ टूट कर चूर हो जाती हैं। |
रासायनिक गुणों पर आधारित विभेद :–
8. वैद्युत अपघटन विधि से धातु का शोधन किस प्रकार किया जाता है?
उत्तर : वैद्युत अपघटन विधि से धातु का शोधन :-
➥ जो धातुएँ क्रियाशीलता श्रेणी के ऊपरी भाग में हैं, अर्थात जो अत्यंत क्रियाशील होती हैं, उन धातुओं को द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके धातुओं को प्राप्त किया जाता है।
उदाहरण : (i) द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्यत अपघटन करके सोडियम धातु प्राप्त की जाती है !
$2NaCl → 2Na^+ + 2Cl^–$
$2Cl^–→ Cl_2 + 2e^–$ ( एनोड पर )
$2Na^+ + 2e^–→ 2Na$ ( कैथोड पर )
______________________________________________________________
$2NaCl → 2Na + Cl_2$
(ii) द्रवित मैग्नीशियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से मैग्नीशियम धातु प्राप्त की जाती है।
$MgCl_2 → Mg^{2+} + 2Cl^–$( एनोड पर )
$2Cl^– → Cl_2 + 2e$ ( एनोड पर )
$Mg^{2+} + 2e → Mg$
__________________________________________________
$MgCl_2 → Mg + Cl_2$
(iii). द्रवित एल्युमिनियम आक्साइड का वैधुत अपघटन करके एल्युमिनियम धातु प्राप्त की जाती है ।
$Al_2O_3 → 2Al^{3+} + 3O^{2–}$ ( एनोड पर )
$3O^{2–} → \frac{3}{2}O_2 + 6e$ ( एनोड पर )
$2Al^{3+} +6e → 2Al$
_______________________________________________________
$2Al^{3+} + 6e → 2Al + \frac{3}{2} O_2$
9. वैसे किन्हीं तीन अधातुई ऑक्साइडों के नाम लिखें जो अम्लीय होते हैं। जल के साथ ऑक्साइडों की अभिक्रिया कैसे होती है?
उत्तर : अम्लीय अधातुई ऑक्साइड :
(i). कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)
(ii). सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂)
(iii). फॉस्फोरस पेन्टाऑक्साइड (P₂O₅)
जल के साथ अभिक्रिया :
अधातुई ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं।
$CO₂ + H₂O → H₂CO₃$ (कार्बोनिक अम्ल)
$SO₂ + H₂O → H₂SO₃$ (सल्फ्यूरस अम्ल)
$P₂O₅ + 3H₂O → 2H₃PO₄$ (फॉस्फोरिक अम्ल)
10. अयस्कों के सांद्रण से क्या समझते हैं? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण आप किस विधि द्वारा करेंगे?
उत्तर : अयस्क का सांद्रण :-
➥ अयस्क में विद्यमान अपद्रव्यों को दूर करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। फेन प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है
इस विधि में अयस्क के भारी चूर्ण को जल से भरी एक टंकी में डालते हैं। तत्पश्चात उस जल में थोड़ा तेल डालकर वायु प्रवाह द्वारा जल को खूब आलोड़ित किया जाता है। विलेय अपद्रव्य जल में घुल जाते हैं और अयस्क के हल्के कण फेन के साथ जल की सतह के ऊपर आ जाते हैं जिन्हें अलग कर लिया जाता है। फेन (झाग) को समाप्त करने के लिए उसमें थोड़ा अम्ल मिलाया जाता है। फिर, सांद्रित अयस्क को छानकर सुखा लेते हैं।
11. अयस्कों के निस्तापन एवं भर्जन से क्या समझते हैं? इनमें अंतर स्पष्ट करें।
उत्तर : निस्तापन :
➥ निस्तापन की प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रवणांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म किया जाता है।
भर्जन :
➥ भर्जन प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को पर्याप्त वायु की आपूर्ति में अयस्क के द्रवणांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म करते हैं।
निस्तापन एवं भर्जन में अंतर :
| निस्तापन | भर्जन |
|---|---|
| (i). इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। (ii). यह ऑक्साइड एवं कार्बोनिट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। |
(i). इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। (ii). यह सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। |
12. कारण बताएँ-
(i) सोना एवं चाँदी का उपयोग आभूषणों के निर्माण में किया जाता है।
(ii) सोडियम धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है।
(iii) ऐलुमिनियम के अतिक्रियाशील होने के बावजूद इसका उपयोग घरेलू बरतन बनाने में किया जाता है।
(iv) मलिन पड़े ताँबा के बरतनों को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है।
उत्तर :
(i) सोना एवं चाँदी धातुएँ बहुत कम क्रियाशील होती हैं, हवा और नमी में भी मलिन नहीं पड़तीं है तथा ये आघातवर्धनीय एवं तन्य होती हैं। इसलिए सोना एवं चाँदी का उपयोग आभूषणों के निर्माण में किया जाता है।
(ii) सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है और वायु की नमी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आकर तुरंत जलने लगता है। किरोसिन में रखने से यह वायु और नमी से सुरक्षित रहता है। इसलिए सोडियम धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है।
(iii) ऐलुमिनियम वायुमंडल के संपर्क में आते ही इसकी सतह पर एक पतली परत Al₂O₃ (ऐलुमिनियम ऑक्साइड) की बन जाती है, जो धातु को ओर अधिक क्रिया करने से रोकती है। इससे यह बरतन बनाने योग्य हो जाता है।
(iv) ताँबा वायु की नमी और CO₂ के संपर्क में आकर बेसिक कॉपर कार्बोनेट [CuCO₃·Cu(OH)₂] की परत बना लेता है। नींबू या इमली के रस में उपस्थित अम्ल इस परत को घोल देता है, जिससे बरतन फिर से चमकने लगते हैं।
13. उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और यह बताएँ कि ये गैसें अक्रियाशील क्यों होती हैं।
उत्तर : उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास :
हीलियम (He) → 2
नीयॉन (Ne) → 2, 8
आर्गन (Ar) → 2, 8, 8
क्रिप्टॉन (Kr) → 2, 8, 18, 8
जेनॉन (Xe) → 2, 8, 18, 18, 8
रेडॉन (Rn) → 2, 8, 18, 32, 18, 8
अक्रियाशील होने का कारण :
उत्कृष्ट गैसों की बाहरी (संयोजक) कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं। इनका संयोजक आवरण पूर्ण होने के कारण ये स्थायी होते हैं। इस कारण ये न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, न ही त्यागती हैं और न ही साझा करती हैं , इसी कारण उत्कृष्ट गैसें रासायनिक दृष्टि से अक्रियाशील होती हैं।
14. रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है?
रासायनिक बंधन :–
➥ वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एकसाथ बाँधकर रखता है, रासायनिक बंधन कहलाता है।
रासायनिक बंधन के प्रकार :–
➥ परमाणुओं के परस्पर संयोग करने की प्रक्रिया के अनुसार रासायनिक बंधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।
(i). वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन :
➥ दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। इसे ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं।
(ii). सहसंयोजक बंधन :
➥ जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है।
सहसंयोजक बंधन तीन प्रकार के होते हैं-
(a). एकल सहसंयोजक बंधन
(b). द्विक सहसंयोजक बंधन
(c). त्रिक सहसंयोजक बंधन
15. वैद्युत संयोजक बंधन क्या है और यह कैसे बनता है?
उत्तर : वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन :–
➥ दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। इसे ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं।
जैसे :–
(i) सोडियम क्लोराइड (NaCl) :–
$Na^+ + Cl^- → NaCl$
कैल्सियम ऑक्साइड (CaO) :–
$Ca^{2+} + O^{2+} → Cao$
सोडियम मोनोऑक्साइड ( $Na_2O$) :–
$Na^{2+} + O^{2-} → Na_2O$
16. सहसंयोजक बंधन से क्या समझते हैं? इसके बनने की प्रक्रिया का उल्लेख करें।
उत्तर : सहसंयोजक बंधन :–
➥ जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है।
सहसंयोजक बंधन तीन प्रकार के होते हैं-
(i). एकल सहसंयोजक बंधन :
➥ जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सिर्फ एक युग्म का साझा होता है तब उनके बीच एकल सहसंयोजक बंधन बनता है।
जैसे :– हाइड्रोजन अणु का बनाना :–
(ii). द्विक सहसंयोजक बंधन :
➥ जब संयोग करनेवाले दोनों परमाणु दो-दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तब उनके बीच द्विक सहसंयोजक बंधन बनता है।
जैसे :– ऑक्सीजन अणु का बनाना :
(iii). त्रिक सहसंयोजक बंधन :
➥ जब संयोग करनेवाले दो परमाणु तीन-तीन (तीन जोड़ा) इलेक्ट्रॉनों (छ: इलेक्ट्रॉन) का साझा करते हैं तब उन परमाणुओं के बीच त्रिक सहसंयोजक बंधन बनता है।
जैसे :– नाइट्रोजन अणु का बनाना
17. निम्नलिखित में सहसंयोजक बंधन बनने की प्रक्रिया का वर्णन करें -
HCI, CCI4, CH4, O₂ और Cl₂
उत्तर : (i). HCl → H के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और Cl के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों अपने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं और एकल सहसंयोजक बंधन बनाते हैं।
(ii). CCl₄ (कार्बन टेट्राक्लोराइड) : C के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और Cl के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है अतः C चार Cl के साथ चार एकल सहसंयोजक बंधन बनाता है।
(iii). CH₄ (मीथेन) → C के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और H के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है अतः C चार H के साथ चार एकल सहसंयोजक बंधन बनाता है।
(iv). O₂ (ऑक्सीजन)
प्रत्येक O में बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः दोनों O दो-दो इलेक्ट्रॉन साझा करके दोहरा सहसंयोजक बंधन बनाते हैं।
(v). Cl2 (क्लोरीन) :
18. आयनिक और सहसंयोजक यौगिकों की विभिन्नताओं का वर्णन करें।
उत्तर : आयनिक और सहसंयोजक यौगिकों में अंतर
| आयनिक यौगिकों | सहसंयोजक यौगिकों |
|---|---|
(i). ये इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं। (ii). ये आयनों से बने होते हैं (iii). ये मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं (iv). इनके द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। (v). ये जल में प्रायः विलेय, किंतु बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि कार्बनिक विलायको में प्रायः अविलेय होते है (vi). विद्युत अपघटन करने पर ये विघटित हो जाते हैं (vii). ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक, किंतु द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। (viii). इनके अणुओं की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। (ix). विलयन में ये तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं |
(i). ये इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझा के फलस्वरूप बनते हैं। (ii). ये उदासीन अणुओं से बने होते हैं। (iii). ये प्रायः ठोस या द्रव होते हैं। (iv). इनके द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। (v). ये जल में अविलेय, किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। (vi). इनका विद्युत अपघटन प्रायः नहीं होता है। (vii). सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। (viii). इनके अणुओं की एक निश्चित ज्यामितिक आकृति होती है। (ix). विलयन में इनकी अभिक्रियाएँ प्रायः धीरे- धीरे होती हैं। |
19. वैद्युत संयोजक यौगिकों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें।
उत्तर : (i). ये इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं।
(ii). ये आयनों से बने होते हैं
(iii). ये मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं
(iv). इनके द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं।
(v). ये जल में प्रायः विलेय, किंतु बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि कार्बनिक विलायको में प्रायः अविलेय होते है
(vi). विद्युत अपघटन करने पर ये विघटित हो जाते हैं
(vii). ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक, किंतु द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं।
(Viii). इनके अणुओं की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है।
(ix). विलयन में ये तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं।
20. सहसंयोजक यौगिकों की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
उत्तर : (i). ये इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझा के फलस्वरूप बनते हैं।
(ii). ये उदासीन अणुओं से बने होते हैं।
(iii). ये प्रायः ठोस या द्रव होते हैं।
(iv). इनके द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं।
(v). ये जल में अविलेय, किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं।
(vi). इनका विद्युत अपघटन प्रायः नहीं होता है
(vii). सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं।
(viii). इनके अणुओं की एक निश्चित ज्यामितिक आकृति होती है।
(ix). विलयन में इनकी अभिक्रियाएँ प्रायः धीरे- धीरे होती हैं।
21. परमाणु संख्या 6, 7 और 8 वाले तत्त्वों की संयोजकता एवं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। इनमें किस प्रकार की संयोजकता है और क्यों?
उत्तर : (i). कार्बन (C) – परमाणु संख्या 6
इलेक्ट्रॉनिक संरचना: 2, 4
संयोजकता: 4
बंधन का प्रकार: एकल सहसंयोजक बंधन, क्योंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन साझा करके अष्टक पूरा करता है।
(ii). नाइट्रोजन (N) – परमाणु संख्या 7
इलेक्ट्रॉनिक संरचना: 2, 5
संयोजकता: 3
बंधन का प्रकार: त्रिक सहसंयोजक बंधन , क्योंकि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन साझा करके अष्टक पूरा करता है।
(iii). ऑक्सीजन (O) – परमाणु संख्या 8
इलेक्ट्रॉनिक संरचना: 2, 6
संयोजकता: 2
बंधन का प्रकार: द्विक सहसंयोजक बंधन , क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन साझा करके अष्टक पूरा करता है।
22. अष्टक नियम क्या हैं? एक आयनिक और एक सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण देते हुए इस नियम को समझाएँ।
उत्तर : अष्टक नियम :
➥ उत्कृष्ट गैसों के अतिरिक्त जितने भी तत्त्व हैं, उनके परमाणुओं के बाह्यतम शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अर्थात इनके संयोजी शेल अपूर्ण होते हैं। इसीलिए इन तत्त्वों के परमाणु अन्य परमाणुओं से संयोग करके उत्कृष्ट गैसों की भाँति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करके बाह्यतम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की स्थायी स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसे अष्टक नियम कहते हैं।
उदाहरण :
(i). आयनिक यौगिक – NaCl (सोडियम क्लोराइड)
Na के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या = 1
Cl के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या = 7
Na इलेक्ट्रॉन त्यागकर Na⁺ बनता है और Cl इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl⁻ बनता है। दोनों के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और अष्टक पूरा होता है।
$Na^+ + Cl^- → NaCl$
(ii). सहसंयोजक यौगिक – H₂O (जल)
O के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या = 6
प्रत्येक H के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या = 1
O अपने 2 इलेक्ट्रॉन H के साथ साझा करता है।
O और H दोनों का बाहरी कक्षा पूरा हो जाता है और अष्टक नियम पूरी होती है।
23. एक तत्त्व A ऑक्सीजन में जलकर एक आयनिक यौगिक AO बनाता है। यदि यह तत्त्व क्लोरीन और गंधक के साथ संयोग करे तब किस प्रकार के यौगिक बनेंगे?
उत्तर : तत्त्व A ऑक्सीजन में जलकर आयनिक यौगिक AO बनाता है। इससे यह स्पष्ट है कि A एक धातु है क्योंकि धातु ही ऑक्सीजन के साथ आयनिक ऑक्साइड बनाते हैं।
(i). क्लोरीन के साथ संयोग –
➥ धातु A, क्लोरीन के साथ क्रिया करके आयनिक धातु क्लोराइड (ACl या ACl₂) का निर्माण करेगा।
$2A + Cl_2 \rightarrow 2ACl$
(ii). गंधक के साथ संयोग –
➥ धातु A, गंधक के साथ क्रिया करके धातु सल्फाइड (AS या A₂S₃) का निर्माण करेगा।
$A + S \rightarrow AS$
अतः ऑक्सीजन के साथ AO, क्लोरीन के साथ ACl या ACl₂ और गंधक के साथ AS या A₂S₃)का निर्माण होगा। ये सभी यौगिक आयनिक प्रकृति के होंगे।
24. वैद्युत संयोजक यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते है, किंतु सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत निम्न होते हैं। ऐसा क्यों होता है?
उत्तर : वैद्युत संयोजक (आयनिक) यौगिकों में धनायन और ऋणायन के बीच मजबूत वैद्युत स्थैतिक बल कार्य करता है। इन आयनों को अलग करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण इनके द्रवणांक और क्वथनांक बहुत ऊँचे होते हैं।
इसके विपरीत, सहसंयोजक यौगिकों में अणुओं के बीच केवल कमज़ोर अंतरा-अणुक बल होते हैं। इन्हें तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत निम्न होते हैं।
25. जस्ता के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखें।
जस्ता (जिंक)
संकेत : Zn
परमाणु संख्या : 30
जस्ता के प्रमुख अयस्क हैं-
(i) जिंक ब्लेंड (ZnS)
(ii) कैलेमाइन (ZnCO3)
(iii) जिंकाइट (ZnO)
जस्ता का निष्कर्षण मुख्यतः कैलेमाइन एवं जिंक ब्लेंड अयस्कों से किया जाता है।
कैलेमाइन से - कैलेमाइन को निस्तापित करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है
$ZnCO_3 → ZnO + CO_2$
कैलेमाइन जिंक ऑक्साइड
जिंक ऑक्साइड (ZnO) को कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करने पर जस्ता धातु प्राप्त होती है
$ZnO + C → Zn + CO↑$
जिंक ब्लेंड से : - सांद्रित जिंक ब्लेंड को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने से जिंक ऑक्साइड (ZnO) प्राप्त होता है।
$2ZnS + 30_2 → 2ZnO + 2SO_2↑$
जिंक ब्लेंड जिंक ऑक्साइड
इस ZnO से उपर्युक्त विधि द्वारा जस्ता प्राप्त कर लिया जाता है
26. पारा धातु का निष्कर्षण कैसे होता है?
उत्तर : . पारा (मरकरी) :–
संकेत – Hg
परमाणु संख्या — 80
पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार (HgS) है जिससे पारा का निष्कर्षण किया जाता है।
सांद्रित सिनेबार अयस्क को चारकोल के साथ गर्म करने पर पारा प्राप्त होता है।
$2HgS + 3O_2 → 2HgO + 2SO_2 ↑$
$HgO + C → Hg + CO ↑$
पारा के वाष्प, CO एवं SO2 के मिश्रण को संघनक से प्रवाहित कर पारा को संघनित कर लिया जाता है।
27. धातुओं के संक्षारण से आप क्या समझते हैं? लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या उपाय हैं?
उत्तर : धातुओं का संक्षारण :—
➥ धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय धातु का संक्षारण कहलाता है।
(i). लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर तेल या ग्रीस का लेप किया जाता है जिससे नमी और ऑक्सीजन का संपर्क रुक जाता है।
(ii). लोहे को पेंट करने से सतह पर परत बन जाती है जो वायु और नमी से बचाव करती है।
(iii). गैल्वनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे की सतह पर जिंक की परत चढ़ाकर उसे जंग से सुरक्षित रखा जाता है।
(iv). लोहे पर क्रोमियम या टिन की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, भी जंग से बचाती है।
(v). लोहे को स्टेनलेस स्टील जैसी मिश्रधातु के रूप में प्रयोग करने से वह जंग नहीं खाता।
28. ऐलुमिनोथर्मिक विधि क्या है? इसकी उपयोगिता बताएँ।
उत्तर : ऐलुमिनोथर्मिक विधि एक धातु अपचयन विधि है, जिसमें एल्युमिनियम को अपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
इस विधि में, धातु के ऑक्साइड को एल्युमिनियम पाउडर के साथ गर्म करके उस धातु को प्राप्त किया जाता है।
$Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Fe + Al_2O_3 + ऊष्मा$
(i). इस विधि से वे धातुएँ प्राप्त की जाती हैं जिन्हें कार्बन द्वारा अपचयन करना कठिन होता है, जैसे — क्रोमियम (Cr), मैंगनीज (Mn), आयरन (Fe), वैनाडियम (V) आदि।
(ii). ऐलुमिनोथर्मिक विधि का उपयोग करके लौह या इस्पात के टुकड़ों को जोड़ने का कार्य किया जाता है।
(iii). यह विधि उच्च तापमान उत्पन्न करने वाली अभिक्रियाओं में प्रयोग की जाती है।
(iv). इस विधि से शुद्ध धातुएँ प्राप्त की जा सकती हैं।
29. बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र लिखें। इसका शोधन कैसे किया जाता है?
बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र :
$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
बॉक्साइट का शोधन :
➥ सांद्रित बॉक्साइट अयस्क को चूना (CaO) की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट (Na₂CO₃) के साथ गर्म किया जाता है।
इससे सोडियम ऐलुमिनेट (NaAlO₂) बनता है —
$Al_2O_3 + Na_2CO_3 \rightarrow 2NaAlO_2 + CO_2 \uparrow$
अब इस मिश्रण को जल (H₂O) के साथ मिलाने पर सोडियम ऐलुमिनेट घुल जाता है, जबकि अशुद्धियाँ नहीं घुलतीं और छानकर अलग कर दी जाती हैं।
छने हुए द्रव में 50–60°C पर कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) प्रवाहित करने से ऐलुमिनियम हाइड्रॉक्साइड [Al(OH)₃] का अवक्षेप बनता है —
$2NaAlO_2 + 3H_2O + CO_2 \rightarrow 2Al(OH)_3 \downarrow + Na_2CO_3$
इस अवक्षेप को छानकर सुखाया जाता है और फिर तेज़ गर्म करने पर यह शुद्ध ऐलुमिनियम ऑक्साइड (Al₂O₃) या ऐलुमिना में परिवर्तित हो जाता है —
$2Al(OH)_3 \xrightarrow{heat} Al_2O_3 + 3H_2O$
अंत में, इस ऐलुमिना का वैद्युत अपघटन करके शुद्ध ऐलुमिनियम धातु प्राप्त की जाती है, जो कैथोड पर जमती है जबकि ऑक्सीजन गैस ऐनोड पर निकलती है।
$Al_2O_3 \rightarrow 2Al^{3+} + 3O^{2-}$
$\text{कैथोड पर : } 2Al^{3+} + 6e^- \rightarrow 2Al $
$\text{ऐनोड पर : } 3O^{2-} \rightarrow \dfrac{3}{2}O_2 + 6e^-$
30. (क) आयनिक और सहसंयोजक यौगिकों में निम्नलिखित गुणों के आधार पर भेद करें :
(i) संघटक तत्त्वों के बीच क्रियाकारी बलों की दृढ़ता
(ii) यौगिकों की जल में बिलेयता
(iii) पदार्थों में वैद्युत चालकता
(ख) स्पष्ट करें कि निम्नलिखित धातुएँ अपने यौगिकों से अवकरण विधि द्वारा किस प्रकार प्राप्त की जाती हैं
(i) धातु M जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित है।
(ii) धातु N जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर की ओर है।
प्रत्येक प्रकार का एक-एक उदाहरण दें।
अथवा
(क) 'भर्जन' और 'निस्तापन' में अंतर लिखें। सल्फाइड अयस्कों के लिए इन दोनों में से किस प्रक्रम का उपयोग होता है और क्यों ?
(ख) एक रासायनिक समीकरण द्वारा रेल पटरियों में दरारों को जोड़ने में ऐलुमिनियम के प्रयोग को स्पष्ट करें।
(ग) अशुद्ध ताँबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण में प्रयुक्त ऐनोड, कैथोड तथा विद्युत अपघट्य के नाम लिखें।
उत्तर : आयनिक एवं सहसंयोजक यौगिकों में भेद :
| क्रम संख्या | गुण | आयनिक यौगिक | सहसंयोजक यौगिक |
|---|---|---|---|
| (i). | संघटक तत्त्वों के बीच क्रियाकारी बलों की दृढ़ता | आयनिक यौगिकों में धनायन व ऋणायन के बीच आकर्षण बल बहुत दृढ़ होता है। | सहसंयोजक यौगिकों में अणुओं के बीच बल कमजोर होते हैं। |
| (ii). | जल में बिलेयता | अधिकांश आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। | अधिकांश सहसंयोजक यौगिक जल में अघुलनशील होते हैं। |
| (iii). | वैद्युत चालकता | आयनिक यौगिक गलित अवस्था या विलयन में विद्युत चालक होते हैं। | सहसंयोजक यौगिक कभी भी विद्युत चालक नहीं होते है । |
उदाहरण:
आयनिक यौगिक — NaCl (सोडियम क्लोराइड)
सहसंयोजक यौगिक — HCl, CH₄ (मीथेन)
(ख). धातुओं की प्राप्ति अवकरण विधि द्वारा :
(i) धातु M : सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित है
जैसे — लौह (Fe), जस्ता (Zn), सीसा (Pb) आदि —
इनके ऑक्साइडों को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अवकृत करके धातु प्राप्त की जाती है।
उदाहरण:
$Fe_2O_3 + 3CO \xrightarrow{heat} 2Fe + 3CO_2$
(ii) धातु N : सक्रियता श्रेणी के ऊपर की ओर स्थित है।
जैसे — सोडियम (Na), पोटैशियम (K), कैल्शियम (Ca), एल्युमिनियम (Al) आदि
ये बहुत अभिक्रियाशील होती हैं। इनके यौगिकों का अवकरण कार्बन द्वारा नहीं किया जा सकता। इन धातुओं को वैद्युत अपघटन द्वारा उनके पिघले हुए लवणों से प्राप्त किया जाता है।
उदाहरण:सोडियम को उसके क्लोराइड से —
$2NaCl \xrightarrow{electrolysis} 2Na + Cl_2$
अथवा (क) उत्तर :
'भर्जन' और 'निस्तापन' में अंतर
| निस्तापन | भर्जन |
|---|---|
| 1. इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। 2. यह ऑक्साइड एवं कार्बोनिट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। |
1. इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। 2. यह सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। |
सल्फाइड अयस्कों के लिए "भर्जन " प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है,
क्योंकि इस प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्कों को ऑक्सीजन में गर्म करने से सल्फाइड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाती है, जिससे धातु निकालना आसान हो जाता है।
उदाहरण :
(ख) उत्तर:
रेल की पटरियों में दरारों को जोड़ने के लिए ऐलुमिनोथर्मिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में ऐलुमिनियम धातु का उपयोग एक अपचायक के रूप में किया जाता है।
इस प्रक्रिया में धातु ऑक्साइड (जैसे – Fe₂O₃) को ऐलुमिनियम पाउडर के साथ गर्म किया जाता है।
ऐलुमिनियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन खींच लेता है और स्वयं ऑक्सीकृत होकर Al₂O₃ बनाता है।
फलस्वरूप लौह पिघले हुए रूप में प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग रेल की पटरियों की दरारें भरने में किया जाता है।
$Fe_2O_3 + 2Al \xrightarrow{heat} 2Fe + Al_2O_3 + \text{ऊष्मा}$
(ग) उत्तर :
ऐनोड: अशुद्ध ताँबा
कैथोड: शुद्ध ताँबे की पतली पट्टी
विद्युत अपघट्य: ताँबे (II) सल्फेट + पतला सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन
Important links :










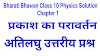




0 Comments